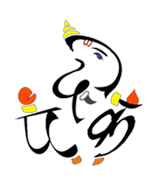गुजरे कहाँ-कहाँ से ( दीपक मिश्र )
यायावरी और सियासत ने कहाँ-कहाँ भटकाया और क्या-क्या दृष्य दिखलाये, कागज में उकेरने बैठता हूँ तो शब्द व भाव, साथ-साथ चलते हुए तो प्रतीत होते हैं किन्तु मिल नहीं पाते, समन्दर के दो किनारों की भाँति। अमीरी के कैलाश को देखा तो उसी की तलहटी में गरीबी की खाई भी मुँह चिढ़ाते नजर आई। बर्फ की गोद में सुलगते कश्मीर का सच जानते हुए भी कहा और लिखा नहीं जा सकता। धर्म और राजनीति का काम नफरत की सर्वग्रासी अग्नि को बुझाना है तो धर्म को आग लगाते और राजनीति को उस आग में घृत डालते देखा तो हतप्रभ होना स्वाभाविक था। मुजफ्फरनगर में अवांछनीय दंगे हुए, दंगें कहीं भी हों दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं, दंगों में न हिन्दू मरता है, न मुसलमान, वहाँ जो लाश गिरती है, वो इंसान और इंसानियत की होती है। साम्प्रदायिकता की आग में इंसानियत के ताने-बाने को ध्वस्त करने का कुत्सित षड़यंत्र किया गया, कुछ हद तक इंसानी लहू पीने वालों की नामुराद टोली को सफलता भी मिली लेकिन समाजवादियों और सद्भावना बनाए रखने वालों के सदप्रयासों की अन्ततोगत्वा जय हुई, साम्प्रदायिक ताकतें हिन्दुओं ;जाटोंद्ध और मुसलमानों को लड़ाने का प्रयास करते रहे लेकिन शामली के फौजी सत्येन्द्र मलिक ने अपने घर पर से अपने मुस्लिम दोस्त रहीसु की बेटी अनवरी का निकाह मुजफ्फरनगर के थाना बुढ़ाना निवासी अख्तर के पुत्र वसीम से करवाकर जवाब दे दिया कि यहां के दिलों के चराग अलग हो सकते हैं पर रोशनी एक है यह वह देश है जहाँ अशफाक-रामप्रसाद ‘‘बिस्मिल’’ और आजाद-भगत सिंह के नाम हमनाम हैं। यह घटना 4 अक्टूबर 2013 की है। स्थिति सामान्य तो हुई किन्तु एक सबक छोड़ गई कि अब और सचेत, सजग, सक्रिय व सावधान रहना होगा। आज भी वो मानसिकता लोगों के जिहन में है जो मानव को एक पल में दानव बना देती है और एहसास तक नहीं होने देती। असली लड़ाई इसी मानसिकता से है, चिन्तन करना पड़ंेगा, उन घटकों को खोजना पड़ेगा, कारणों के तह में जाना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि क्यों सदियों से हम हर साल ‘रावण’ को जलाते आ रहे हैं और न ‘रावण’ मर रहा है, न रावणी मनोवृत्ति व राक्षसी प्रवृत्ति कम हो रही है। दंगों की मानसिकता को खत्म करना नितान्त आवश्यक है, प्रीत की गंगा-यमुना व सरस्वती के संगम के ऊपर स्याह घनेरा गहराता जा रहा है, हिन्दुस्तान का किश्तों में रोज कत्ल हो रहा है। कहीं रज्जो, सलमा, लक्ष्मीअम्मा के रूप में भारत माता की लाश गिर रही है तो कहीं धनुआ, रमजान, सुखविन्दर के रूप में हिन्दुस्तान के सीने में खंजर उतर रहा है। दंगे करने वाले लोग, घर और जिन्दा इंसान को आग में जलाने वाले लोग न हिन्दू हो सकते हैं न मुसलमान। मुसलमान तो मुर्दा तक नहीं जलाता और हिन्दू संस्कृति तो साँप तक को दूध पिलवाती और पत्थर तक को पुजवाती है।
यह नहीं कि नाव की ही जिन्दगी खतरे में है,
सच तो यह है कि पूरी नदी खतरे में है,
न नानक, न मूसा, न राम, न मसीह,
पूजता है जो इन्हें वो आदमी खतरे में है।
इन खतरों की चुनौतियाँ किसी एक क्षेत्र, जाति, सम्प्रदाय या भाषा से जुड़े वर्ग के ही समक्ष नहीं है, पूरी मानवता के समक्ष है, जिसमें हम भी हैं और आप भी। जब तक हर हिन्दू कबीर, रहीम, हजरत निजामुद्दीन औलिया, अशफाकउल्ला खान, भगत सिंह सदृश पूर्वजों का स्वयं को वंशज नहीं मानेगा और हर मुसलमान राम, कृष्ण, गौतम, लोहिया को अपना अजदाद नहीं समझेगा, ये अलगाव व नफरत की आग लगती रहेगी, देश थोड़ा-थोड़ा करके जलता रहेगा, एक दिन सब कुछ जल कर खाक हो चुका होगा, तब हम पश्चाताप करने के भी हकदार नहीं होेंगे, सिर्फ शर्मसार होंगे। दुनिया दिन-ब-दिन सांवेगिक दृष्टिकोण से छोटी होती जा रही है। भावनायें, निष्ठायें और आदर्श संकुचित होते जा रहे हैं। हम 20वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में आजाद हुए, यहाँ अपना निजाम स्थापित हुआ। होना तो यह चाहिए था कि अपनी संस्कृति व विरासत की रोशनी में हम अपने मूल्यों को और अधिक विस्तार देते, लेकिन हुआ उल्टा, हम चले तो जरूर लेकिन विपरीत दिशा में, परिणाम सामने है कि हमारी सोच छोटी हो गई है और हम आदमकद नहीं रहे, बौने हो गये। साहित्य की तरह सिनेमा भी समाज का दर्पण है, यूँ कहें कि समाज, साहित्य, संगीत, सियासत, सहाफत, सिनेमा, समसामयिक सोच व समझ, सब एक दूसरे के पैरों से चलते हैं। साठ के दशक में जब हमारी सोच बड़ी होती थी, तब के संगीत व गीतों में भाव भी बड़े उदात्त व व्यापकता के द्योतक होते थे। ‘‘युग-युग से हम गीत मिलन के गाते रहेंगे’’, ‘‘जनम-जनम का साथ है हमारा तुम्हारा-तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जनम दोबारा’’, का स्थान ‘‘कोई रात मेरे साथ गुजार सुबह तक करुँगा प्यार’’ जैसे गीतों ने ले लिया। वो ‘‘प्रीत’’ जिसका विस्तार कई युगों व जन्मों तक होता था, अब एक रात या कुछ घण्टों तक सिकुड़ एवं सिमट कर रह गई। मोहब्बत जो इबादत होती थी, अब ‘‘जस्ट प्ले’’ और ‘‘हर एक दोस्त कमीना’’ हो चुका है। अब दोस्त हमदम, हमदर्द हमसखुन, हमनशीं नहीं रहे। फिल्मी गीतों से इसी सोच के समाज का पता चलता है। यह भावगत संकुचन हर तरफ प्रतिबिम्बित है। अब पीपल, बरगद, नीम, गुलमोहर, अशोक का स्थान वृक्षों में कैक्टस, यूकेलिप्टस जैसे पेड़ों ने ले लिया। हम किस भी शहर में टहल कर देख सकते हैं। ‘‘निरस्तपादवे अरण्यऽपि द्रुमायते’’। राजनीति में लोहिया, जयप्रकाश सरीखे व्यक्तित्व नहीं दिखते, पत्रकारिता में ‘‘विष्णु राव पराड़कर’’ का अभाव है। यह सँकुचन आर्थिक सँकुचन से ज्यादा भयावह और आत्मघाती है। हम या तो आत्ममुग्ध है या शोकमग्न, दोनों परिस्थितियाँ समाज, देश व दुनिया के लिए आत्मघाती हैं। कश्मीर में डल झील में नौकायन करते हुए मेरे मन में था कि यहाँ रहने वाले लोग कितने सुखी हांेगे, चारो तरफ सुन्दर दृश्य, सुहावना वातावरण, मैं कश्मीरियों के प्रति द्वेषभाव से स्वयं को ग्रसित पा रहा था। डल झील के मध्य में एक होटल है, होटल पर काम करने वाले बुजुर्ग अशरफ से पूछा कि आप लोग तो यहाँ काफी मजे में रहते होंगे क्योंकि यहाँ जैसी सुन्दरता कहीं नहीं मिलती। उसने बड़े ही उदास मन से कहा कि साहब यह जिन्दगी भी कोई जिन्दगी है, चारो तरफ केवल पानी और पहाड़, साहब ठहरी हुई चीज अच्छी नहीं होती। उस 65 वर्षीय अनपढ़ बुजुर्ग के एक वाक्य के आगे कई किताबों के अध्ययन का ज्ञान भी छोटा लग रहा था। हमारे देश में जाति प्रथा, दहेज प्रथा, साम्प्रदायिकता, जैसी बीमारियाँ आ के यहीं ठहर गई हैं, उनका ठहरना पूरे देश के प्रवाह को कुप्रभावित कर रहा है। ‘‘चरैवति चरैवति’’ का उद्घोषक भारत पिछले एक दशक से विकास क्रम में 135-137 के पायदान पर ठहरा हुआ है। जब दुनिया द्रुतगति से चल रही हो, हमारा ठहराव उचित नहीं। 2 अक्टूबर 2014 को महाराष्ट्र के समाजवादियों ने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, मुझे बतौर प्रशिक्षक भेजा गया। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है जहाँ ऐसी ऊँची गगनचुम्बी अट्टालिकायें हैं कि नीचे से खड़ा होकर देखा नहीं जा सकता, पूरी गरदन टेढ़ी करने के बाद भी पीठ को पीछे के ओर झुकाना पड़ता है, तब जाकर इन भवनों की ऊपरी माला ;तल्लाद्ध दिखती है। अमिताभ, अम्बानी, लता, तेन्दुलकर की मुंबई में सुबह मैं टहलने निकला तो देखता हूँ कि एक 22 तल्ले की बिल्डिंग के नीचे एक भिखारीनुमा व्यक्ति कूड़े के ढे़र से पाव बीन कर खा रहा है, उसके चेहरे पर धूप और धूल की इतनी परतें जम चुकी हैं कि अंदाज लगाना मुश्किल था कि उसका रंग कैसा रहा होगा?उसका उबलते हुए गन्ने के झाग जैसा रंग गटर के काले पानी जैसा मलिन हो चुका था। वो जहाँ पाव बीनकर खा रहा था, उसी कूड़े के ढ़ेर पर बैठी एक कुतिया अपने पिल्लों को दूध पिला रही थी और थोड़ी दूरी एक सुअर अपनी पाली का इंतजार कर रहा था कि दोनों हटें तो वह आकर कुछ खाये। मैं वहाँ की बदबू को सह पाने की स्थिति में नहीं था, 20 रुपए की पाव-रोटी खरीद कर तीन भाग में बाँट कर एक भाग कुतिया की तरफ, दूसरा भाग सुअर की तरफ और तीसरा भाग उस व्यक्ति ;जो इन दोनों से बदतर स्थिति में थाद्ध की ओर फेंका, वह आदमी इस तरह से पाव-रोटी पर टूटा जैसे महीनों से भूखा हो। संभवतः ऐसा ही दृश्य देखकर कविवर ने लिखा होगा -
‘‘लपक चाटते जूठा पत्तल जिस दिन देखा नर को,
सोचा क्यों न आग लगा दूँ आज मैं दुनिया भर को।’’
जब तक ऐसे दृश्य दुनिया में रहेंगे, दुनिया में शांति असम्भव है। जब मुम्बई का यह हाल है तो बाकी क्षेत्रों की कल्पना की जा सकती है। आज भी ऐसे गरीबों की संख्या करोड़ों में है जिनके लिए जिन्दगी की परिभाषा मौत को टालते जाना है, जिनके पैरों के नसीब में छाले और ऐसे रास्ते हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं। राजनीति का काम जो विसंगतियाँ समाज में व्याप्त हैं, उन्हें परिष्कृत कर ‘‘सत्यम् शिवम् सुन्दरम्’’ की स्थापना करना है, सामाजिक संकुचन तथा क्षरण को रोकना है लेकिन लग रहा है कि सियासत खुद ही विकृतियों और विसंगतियों के कारण पंगु हो गई है। सभी मनीषियों का मत है कि राजनीतिक व्यक्ति को कभी भी धन-संचय नहीं करनी चाहिए। उसका जीवन-दर्शन उस बादल जैसा होना चाहिए जो समन्दर से प्राप्त नीर को मरुस्थल को देते हुए अनंत यात्रा में लीन हो जाता है। गांधी-लोहिया की जीवन दर्शन इसका उदाहरण है। आज राजनीति में आने वाले युवा एक दो साल में ही कारों की कतारों व गार्ड-गनर के फेर में पड़ जाते हैं, विचार व किरदार की बजाय उनकी पहचान, उनका पहनावा और वो साधन हो गया है जिससे चलते हैं। दुर्भाग्य है कि यह बीमारी उन दलों को भी लग गई जो हमेशा बाह्य आडम्बरों के खिलाफ रहे। मैंने लगभग पूरे देश का भ्रमण किया है, कई संवाद और परिचर्चाओं का आयोजन किया, और महसूस किया है कि पूरे देश के बुद्धिजीवियों को अरण्यरुदन की आदत हो गई है, वे सरकार की चादर ओढ़कर सोने के आदी हैं, वातानुकूलित कक्ष में वातावरण को बदलने की चर्चा तथा नेताओं की शिकायत उनका फलसफा बन गया है। उनकी उदासीनता देश के लिए उचित नहीं। एक समय था कि देश का सर्वोच्च दिमाग राजनीति करता था, तब राजनीति वैचारिक होती थी और उसकी विश्वसनीयता असंदिग्ध थी, अब कैसे लोग राजनीति में प्रभावी है, सर्वविदित है। एक अभियान चलाकर राजनीति और सामाजिक गतिविधियों के प्रति आई उदासीनता को दूर किए बिना देश का भला नहीं होगा। इन दिनों हम समाजवादी लोग हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए अभियान चला रहे हैं। इसके लिए चिन्तन सभा के ही अन्तर्गत उपनिवेशवादी विरोधी मोर्चा का गठन किया गया, पूूरे देश से लोग हमारे हस्ताक्षर अभियान का न केवल समर्थन दे रहे हैं अपितु इसमें सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं। बंगलाभाषी कृष्ण कुमार सिंघानिया, हरियाणवी भाषी सुखबीर सिंह हुड़ा, कश्मीरी बोलने वाले फय्याज अहमद भट्ट जैसे साथी तो इस अभियान में मुझसे भी अधिक सक्रिय हैं। मैंने 18 प्रांतों की यात्रा इस मिशन का परचम लेकर किया, जो समर्थन, सम्मान और स्नेह मिल रहा है, उत्साहित हूँ। यूएनओ के एक बड़े अधिकारी ने वार्ता के दौरान कहा कि हिन्दी के भारत में अन्य भाषायी लोग विरोधी हैं, उन्हें जब अभियान के दौरान अर्जित अनुभवों को बतलाऊँगा तो वे चैंक जायेंगे और अपने पूर्वाग्रह को बदल देने के लिए विवश होंगे। हिन्दी का सभी प्रांतों के लोग उतना ही मान रखते हैं जितना अपनी मातृभाषा का, वे अपनी मातृभाषा को माँ तो हिन्दी को ‘बड़ी मौसी’ समझते हैं। हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की पहली बार माँग कवि नर्मद ने की थी, जो गुजराती कवि थे। इसके प्रबल पैरोकारों में अग्रगण्य तिलक व गोखले मराठी, महात्मा गाँधी गुजराती, भगत सिंह पंजाबी व नेताजी सुभाषचंद्र बोस बंगला भाषी थे। जब तक हिन्दी को यूएनओ की आधिकारिक भाषा का दर्जा और हिन्दुस्तान को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता नहीं मिलेगी, भारत को वो वैश्विक सम्मान नहीं मिल सकेगा, जिसका वो पात्र है। डा0 मनमोहन सिंह ने न जाने क्यों इन मुद्दों को कभी प्रभावशाली तरीके से नहीं उठाया, उनसे उम्मीद करना भी बेकार है, यूकेलिप्टस से छाया और फल की उम्मीद करने जैसा है।
अन्ततोगत्वा, इतना ही कहूँगा कि सिर्फ चुनाव लड़ना, सांसद विधायक व मंत्री बनना ही राजनीति नहीं है, राजनीति नीति बनाने और नेतृत्व प्रदान करने का मंच है, इसे भौतिक चमक से बचाना और सैद्धान्तिक धरातल के समीप रखना नितान्त आवश्यक है, समाजवाद व सामाजिक सद्भाव एक लोकधर्म है। यह पूरी दुनिया को एक गांव और एक परिवार (वसुधैव कुटुम्बकम) में बदलने का उद्घोष करती है न कि बाजार बनाने की जिसमें सिर्फ वह रहे जिसके पास क्रयशक्ति और पाकेट में पैसा हो, हमारी राजनीति ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त ‘‘संगच्छध्वं संगवदध्यं’’ से प्रारम्भ होती है, ‘‘समाना वः आकृति, समाना व हृदयानिवां ‘‘सहचित्तमेषाम्’’ ‘‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’’ ‘‘समाज देवो भवः’’ ‘‘सहनाववतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे’’ एक ही ‘सफ में खड़े महमूद-ओ-अयाज़, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदानवाज़’ जैसी भावनाओं व विचारों को समेटती हुई लोहिया की सप्तक्रांति तक पहुँची है, इस विरासत को बचाए रखने की चुनौती हमारे समक्ष है।
‘‘गमों की आंच पर अश्कों को उबालकर देखो,
बनेंगे रंग किसी पर भी डालकर देखो।
तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी,
किसी के पांव का काँटा निकाल कर देखो।’’